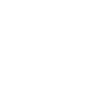सप्तम अध्याय -- उच्चैःश्रवा तथा औच्चैःश्रवा
सप्तम अध्याय

उच्चैःश्रवा तथा औच्चैःश्रवा
निघण्टु के 26 अश्वनामों में उच्चैःश्रवा अथवा औच्चैःश्रवा की गणना भी की गई है । निघण्टु की कुछ पाण्डुलिपियों में प्रथम नाम आता है और कुछ में दूसरा; परन्तु दोनों नामों का प्रयोग यहाँ बहुवचन में हुआ है । पुराणों में देवराज इन्द्र के घोड़े का नाम उच्चैःश्रवा है जो समुद्र-मन्थन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक है। ब्रह्माण्ड पुराण (3.3.76, 8.10) तथा मत्स्यपुराण (8.8) में उच्चैःश्रवा गान्धर्वी का पुत्र है जो अन्य सब घोड़ों का राजा होता है । वायुपुराण(76-73) के अनुसार वह भद्रा से उत्पन्न एक घोड़ा है । वेद में उक्त दोनों नाम एकवचन में प्रयुक्त हुए हैं।
श्रवस्
इन दोनों नामों पर वैदिक दृष्टि से विचार करने से पूर्व श्रवस् शब्द को समझ लेना आवश्यक है जो इन दोनों नामों में उत्तरपद के रूप में विद्यमान है । श्रवस् शब्द श्रु धातु के संप्रसारण को प्रस्तुत करता है जहाँ श्रु धातु कानों द्वारा सुने हुए बाह्य शब्द-ग्रहण की द्योतक है। वहीं उसके संप्रसारण के द्वारा जो श्रव धातु बनती है वह न केवल सभी ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषय-ग्रहण की ओर संकेत करती है अपितु वह ज्ञाननेत्र के द्वारा आन्तरिक ज्योति आदि के ग्रहण का भी बोध कराती है । इस श्रव धातु से निष्पन्न श्रवस् शब्द निघण्टु के अन्न नामों और धननामों में परिगणित है। डॉ. श्रद्धा चौहान ने अपने शोध-प्रबन्ध1 में वेद के धन नामों पर लिखते हुए श्रवस् सहित सभी प्रकार की अध्यात्मिक शक्तियों का द्योतक माना है ।
वेद में श्रवस् शब्द के लिए प्रायः ‘बृहद्द्युम्नम'2 विशेषण का प्रयोग हुआ है। इससे स्पष्ट है कि वह कोई ज्योतिर्मयी बृहद् वस्तु है । कभीकभी उसको ज्येष्ठं और ओजिष्ठम् (ऋ. 6.37.3) तथा महान् श्रवस् महिश्रवः' (ऋ. 1.79.4; 5.18.5) भी कहा जाता है । श्रवस् सूरी अथवा विचक्षण कहे जाने वाले ज्ञानियों से सम्बन्ध रखता3 है । एक मन्त्र में आन्तरिक समुद्र में चलने वाली हिरण्ययी नौकाओं का उल्लेख है जिनके द्वारा सूर्य का दौत्य कर्म करता हुआ पूषा श्रवस् की इच्छा करता है ।4 वे
---------------------------------
1 जोधपुर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच.डी. के लिए स्वीकृत 'ऋग्वेद में धन की - परिकल्पना' शीर्षक निबन्ध [अप्रकाशित] ।
2 ऋ. 1.9.8 और 3.37.10 इत्यादि
3 ऋ. 5.86.6; 6.2.1
4 वही, 6.58.3
86
हिरण्ययी नौकाएँ हिरण्ययकोश से उद्भूत ज्योति की धाराएँ हैं जो मनुष्य-व्यक्तित्व का पोषण करने के लिए प्रवाहित होती हैं । अतः इनसे यात्रा करने वाला पूषा तत्त्व जिस श्रवस् की कामना करता है वह भी कोई आध्यात्मिक तत्व होना चाहिए। अन्यत्र अग्नि से प्रार्थना की गई है कि वह इन मर्त्यों में ‘द्युम्नं श्रवस्'1 तथा 'चित्तं' प्रदान करें क्योंकि वह श्रवस् ‘अमृत्यु2 (मृत्युरहित ) है । यह श्रवस् वस्तुतः अमर्त्यों में है जिसकी इच्छा और याचना करते हुए ऋभुओं को तेज से स्पन्दित मनुष्य-व्यक्तित्व रूपी एक पात्र को विशेष रूप से क्षेत्र की तरह निर्माण करते हुए बताया3 गया है। एक स्थान पर ज्ञानाग्नि (अग्निवेधस्) से प्रार्थना की गई है कि उसकी अभिव्यक्तियाँ हमारे मन और हृदय के लिए प्रीतिकर हों और हम देवों में विभक्त श्रवस् प्राप्त करते हुए संयम रूपी धन को प्राप्त कर सकें ।4
श्रवस् की दिव्यता अथवा आध्यात्मिकता का संकेत ऐसे अनेक विशेषणों से भी मिलता है जो देवपुरी अयोध्या (मनुष्य-व्यक्तित्व) के देवों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। चित्रश्रवस्तम विशेषण अग्नि के लिए (ऋ. 1.1.5) तथा ‘वृत्रहन्तम' इन्द्र के लिए (ऋ. 8.92.17) तो प्रयुक्त हुए ही हैं; परंतु एक स्थान पर रयिनामक अध्यात्मिक धन को भी ‘चित्रश्रवस्तम'5 कहा गया है। सोम सुश्रवस्तम है और ‘सुक्षिति सुश्रवस्तमं जयन्तम्'6 को जीतने वाला7 है । इस प्रकार अग्नि, इन्द्र और सोम के साथ जिस श्रवस् का विशिष्ट सम्बन्ध है वह अवश्य कोई अध्यात्मिक तत्त्व ही हो सकता है क्योंकि वेद में अग्नि, इन्द्र तथा सोम में से प्रत्येक स्वयं प्रमति है तथा उसे मतियों आदि का देने वाला8 कहा गया है। सूर्य की दुहिता देवों में जिस ‘श्रवः अमृतम् अजुर्यम्' का विस्तार करती हुई (ऋ. 3.43.15) कही जाती है वह नि:सन्देह उस श्रवस् से भिन्न है जिसे ससर्परीवाक् पाञ्चजन्य कृष्टियों (ऋ. 3 .53.16) में भरती है । प्रथम श्रवस् को ही अन्यत्र ‘उत्तमं श्रव वर्षिष्ठम्' कहा गया है जिसे सूर्य हमारे देवों में अस्माकं देवेषु'9 उत्पन्न करता है जबकि दूसरे को, वीरवत् श्रवस् माना जा सकता है; जिसका ऋभुओं द्वारा यहाँ (इह) हमारे लिए तक्षण किया10 जाता है । यह
---------------------------------
1 आ एषु द्युम्नम् उत श्रव आ चित्तम् मर्त्येषु धाः । वही, 5.7.9
2, वही, 6.48.12
3 वही, 1.110.5
4 वही, 1.73.10
5 वही, 7.24.3
6 वही, 1.11.17
7 1.91.21
8 डा. फतहसिह के अनुसार, अग्नि, इन्द्र, सोम क्रमशः ज्ञानपरक प्रमति, क्रिया
परक प्रमति तथा भावनापरक प्रमति के रूप में आत्मा के अंगभूत हैं ।
9 ऋ. 4.31.15 .
10 वही, 4.36-7
87
द्विविध प्रकार का श्रवस् नि:सन्देह एक तो हमारे अमृत-स्तर से सम्बन्ध रखता है और दूसरा मर्त्य स्तर पर जहाँ ज्ञानेन्द्रिय के रूप में पञ्चकृष्टियां कार्यरत हैं । अतः प्रथम को हमारी अतीन्द्रिय दिव्य शक्तियों से प्राप्त अनाहतनाद युक्त ज्ञान कहा जा सकता है और द्वितीय को ज्ञानेन्द्रियों से प्राप्त अनुभव माना जा सकता है । इस दृष्टि से जहाँ प्रथम को निघण्टु में स्वीकार कर सकते हैं, वहाँ दूसरे को निघण्टु के अन्न बोधक श्रवस् के रूप में लिया जा सकता है। इन्द्रियानुभवजन्य ज्ञान हमारे अन्तःकरण का अन्न है ।
प्रथम अश्विनौ द्वारा धारण किया हुआ ‘प्रवाच्यं श्रव' (ऋ.1.117-8) है, तो द्वितीय शरीर1 को (असुरस्य) इन्द्रिय रूपी गायों का वह ‘शतं श्रवस्' है जिसे कक्षीवान् ऋषि2 प्रसारित करते हैं। इन दोनों में से प्रथम श्रव को उच्चतर तथा दूसरे को निम्नतर कहा जा सकता है । इसी दृष्टि से वेद में उच्चैःश्रवा और औच्चैःश्रवा की कल्पना की गई प्रतीत होती है, जिनका समुचित विवेचन करने के लिए ही यहाँ श्रवस् शब्द की कुछ मीमांसा की गई है । अतः इन दोनों अश्व नामों पर विचार किया जा रहा है—
उच्चैःश्रवा और औच्चैश्रवा :
इन दोनों नामों का उल्लेख इन्द्र के दो प्रसिद्ध हरियों के नामों की भाँति ऋग्वेद के एक खिलसूक्त3 में हुआ है । वह खिल दाशराज्ञ युद्ध में इन्द्र के पराक्रम की गाथा से प्रारम्भ होता है। इन्द्र द्वारा दाशराज्ञ युद्ध में जिस ‘अमानुष' का विगाहन हुआ उसी को वहाँ विरूप, विषाक्ष, रोहिण तथा वृत्र आदि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस इन्द्र ने पर्वतों को स्थिर किया और आपः को मुक्त किया उस वृत्रहन् को नमस्कार करते हुए, उक्त खिलसूक्त में इन्द्र के दो हरियों में से सर्वप्रथम दौड़ते हुए औच्चैःश्रवस् का उल्लेख किया गया है । उसको ‘स्वस्त्यश्व' कह कर सम्बोधन करते हुए उससे विजय के लिए (जैत्राय) इन्द्र तथा रथ को वहन करने के लिए कहा गया है--
प्रष्टि धावन्त हर्योरोच्चैःश्रववसमब्रवम् ।
स्वस्त्यश्व जैत्रायेन्द्रमा वहतो रथम् ।। (खि. 5.14.4)
---------------------------------
1 डॉ. फतहसिह के अनुसार, मनुष्य-व्यक्तित्व में शरीर असुर स्तर है और आत्मा देव-स्तर (देखिए, वैदिक दर्शन)
2 ऋ 1.126.2
3 खि 5.14
88
यही मन्त्र अथर्ववेद में घोड़े से पाठ भेद के साथ उसी प्रकार प्रस्तुत किया गया है –
पृष्ठं धावन्तं हर्योच्चैःश्रवसमब्रुवन् ।
स्वस्त्यश्व जैत्रायेन्द्रमा वह सुस्रजम् ।। (अथर्व. 20.128.15)
इस मन्त्र के अनुसार औच्चैःश्रवस् से कहा जा रहा है, वह पीठ की ओर दौड़ रहा है तथा उसे मालाधारी इन्द्र को जैत्र' नामक रथ के लिए वहन करना है। इसके विपरीत इन्द्र के दोनों हरियों में जो दूसरा घोड़ा है उसका उच्चैःश्रवा नाम है। उसके विषय में खिलसूक्त का यह मन्त्र द्रष्टव्य है--
यत्वा श्वेता उच्चैःश्रवसं हर्योर्युञ्जन्ति दक्षिणम् ।।
मूर्धानमश्वं देवानां बिभ्रदिन्द्र महीयते ।। (खि. 5.14.5)
यही अथर्ववेद में कुछ भेद के साथ इस प्रकार पाया जाता है
ये त्वा श्वेता अजैश्रवसो हार्यो युञ्जन्ति दक्षिणम् ।
पूर्वा नमस्य देवानां बिभ्रदिन्द्र महीयते ।। (शौ. 20.128.16)
खिल और अथर्ववेद दोनों के अनुसार हरियों में से दक्षिण हरि को श्वेत उषाएँ रथ से जोड़ती हैं ; परन्तु इस दक्षिण अश्व का नाम खिल के अनुसार उच्चैःश्रवा है, जबकि अथर्ववेद में अजैश्रवा कहा गया है। सम्भवतः अथर्ववेद का अजैश्रवा नाम उच्चैःश्रवा का भ्रष्ट पाठ प्रस्तुत करता है। खिलसूक्त के अनुसार उच्चैःश्रवा देवों का मूर्धा (श्रेष्ठ) अश्व है, जो इन्द्र को धारण करते हुए महिमावान् होता है । इस अश्व को हम पूर्वोक्त अमृतं श्रवस् से युक्त मान सकते हैं, जिसे मनुष्य-व्यक्तित्व के अमृतस्तर की वस्तु माना गया है। इसी उच्चश्रवस् से युक्त होने के कारण उसका नाम उच्चैःश्रवा है और इसीलिए उसको दक्षिण तथा मूर्धा अश्व कहा जाता है । इसके विपरीत पीछे को दौड़ने वाला पूर्वोक्त औच्चैःश्रवा उसी श्रवस् के निम्नतर मर्त्यस्तर से सम्बद्ध तत्त्व प्रतीत होता है। दूसरे अश्व को पहले का एक रूपान्तर ही समझा जाता था। इसलिए उसको उच्चैःश्रवा का अपत्य स्वीकार करके उसको औच्चैःश्रवा नाम दिया गया।
इस प्रसंग में एक बात और विचारणीय है कि उच्चैःश्रवा अश्व जहाँ रथरहित इन्द्र को धारण करता है, (बिभ्रदिन्द्रिम्) वहाँ औच्चैःश्रवा का सम्बन्ध केवल रथयुक्त इन्द्र से ही है। डॉ. फतहसिंह के अनुसार वेद में रथ मनुष्य-व्यक्तित्व का द्योतक है जबकि वह मनुष्य-रथ आत्मारूपी इन्द्र की उपाधि है । अतः आत्मा रूपी इन्द्र के निरुपाधिक स्वरूप को ही रथविहीन कहा जा सकता है। इन्द्र के इसी स्वरूप को वेद में शुद्ध इन्द्र भी कहा गया है --
89
इन्द्र शुद्धो हि नो रयिं शुद्धरत्नानि दाशुषे ।
शुद्धो वृत्राणि जिघ्नसे शुद्धो वाजं सिषाससि ।। ऋ. 8.95.9
यह शुद्ध इंद्र ही रयि तथा रत्नों का देने वाला है। यही वृत्रों का हनन करता है तथा वाज नामक शक्ति भी प्रदान करता है । उक्त मन्त्र से पूर्व ही शुद्ध इंद्र का आह्वान शुद्ध ऊतियों के साथ आने के लिए किया गया है। यह शुद्ध इंद्र रयि को धारण करता है और सौम्य होने से मादकता देता है--
इन्द्र शुद्धो न आ गहि शुद्धः शुद्धाभिरूतिभिः ।
शुद्धो रयिं निधारय शुद्धो ममद्धि सोम्यः । ऋ. 8.95.8
जैमिनीय ब्राह्मण 3.228 के अनुसार असुरों की हत्या करने के कारण इंद्र अपने को अमेध्य और अपूत मानने लगा था। इसलिए उसने इच्छा की कि मेरे शुद्ध होने पर शुद्ध सामगान द्वारा मेरी स्तुति की जाए।
ऋषियों ने जिस साम के द्वारा उस इद्र की स्तुति की वह निम्नलिखित हैक—
एतो न्विन्द्रं स्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना ।
शुद्धैरुक्थैर्वावृध्वासं शुद्ध आशीर्वान् ममत्तु ।। ऋ. 8.95.7
इस विवरण से स्पष्ट है कि आत्मा के निरुपाधिक स्वरूप से सम्बन्धित किसी तत्त्व का नाम ही उच्चैःश्रवा है। उसके विपरीत सोपाधिक आत्मा से सम्बन्धित उसी के रूपान्तर को औच्चैःश्रवा माना गया है। महर्षि अरविन्द ने इंद्र के इन दोनों अश्वों को दो अन्तर्दृष्टियाँ कहा है। इसमें एक दक्षिणादृष्टि है और दूसरी सव्या1 ।
डॉ. फतहसिह ने इंद्र के इन दोनों अश्वों को क्रमशः ज्ञानमयी और भावनामयी अन्तर्दृष्टियाँ कहा है। उसकी पुष्टि में एक ब्राह्मणवचन2 को उद्धृत करते हुए उन्होंने एक को ऋक् और दूसरे को साम माना है; परन्तु वे दोनों शक्तियाँ उनके अनुसार विज्ञानमयकोश तक ही रहती हैं, जबकि हिरण्ययकोश में दोनों हरियों के स्थान पर एक ही हरि रह जाता है। वह स्वयं इंद्र से अभिन्न होता है। इस अद्वैत अवस्था को चित्रित करते हुए तथा सर्वहरि रूप में इन्द्र की कल्पना करते हुए ऋग्वेद का 10.96 सूक्त विशेष रूप से द्रष्टव्य है। इसमें हरि नामक योनि में (जिसे 'दिव्यं सदस्' कहा गया है) सारी अनेकता समाहित हो जाती है (मन्त्र 2) और उसका जो वज्र पहले ‘आयस' कहा जाता था, वह अब ‘हरिः निकामः' अथवा
---------------------------------
1 Hymns to the Mystic Fire P. 311; Foot Note-2
2 ऋक्सामे वै हरी-माशबा 4.4.3.6
90
हरि कहा जाता है और वह स्वयं इंद्र ही है, जिसमें हरित कहलाने वाले सभी तत्त्व लीन हो जाते हैं --
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गभस्त्योः ।
द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इंद्रे निरूपा हरिता मिमिक्षिरे ।। ऋग्वेद 10.96.3 इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि इस सूक्त के मन्त्र 11 में, अवर इंद्ररूपी असुर से प्रार्थना की गई है कि वह हरिरूपी सूर्य के लिए गो के कमनीय गृह को आविर्भूत करे--
‘प्र पस्त्यमसुर हर्यतं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ऋ. 10.96.11
यह कमनीय गृह वस्तुतः हिरण्ययकोश रूपी ज्योतिर्मण्डित स्वर्ग है जिसमें आत्मा से युक्त ब्रह्म भी विराजमान होता है। हिरण्ययकोश ही उस परावाक् रूपी गो का कमनीय गृह है जो विज्ञानमय कोश में ऋक्सोमात्मक दो हरियों के रूप में होती है; परन्तु इस (हिरण्यय) कोश में यजुः मात्र होकर सारी अनेकता को एकीभूत1 करने वाली कही जाती है । हिरण्ययकोश का यजुः ब्रह्मवाक् भी है और स्वयं ब्रह्म भी, क्योंकि वहाँ एक ही अद्वैत तत्त्व रह जाता है जिसे कभी सभी भूतों को जोड़ने वाला यजुब्रह्म3 कहा जाता है और कभी इदं सर्वं को जन्म देने वाला यजुर्वायु2 कहा जाता है। आरोहण-क्रम में मनुष्य-व्यक्तित्व की समस्त अनेकता जिस यजु: में एकीभूत होती हैं अवरोहण क्रम में वही यजुः उस अनेकता को उगल देती है।
यह द्विविध गति वस्तुतः विज्ञानमय कोश में होती है। डॉ. फतहसिंह ने आगमों के आधार पर अपने वैदिक4 दर्शन में इसी को उन्मनी-समनी भेद से दो प्रकार की शक्ति माना है । उन्मनी रूप में हिरण्ययकोश में जाकर वही सच्चिदानन्दमयी परावाक् हो जाती है और समनी रूप में वही मनोमय कोश की अनेकतामयी सृष्टि का रूप धारण कर लेती है । प्रथम रूप में, वह मनोमय की अनेकता का हरण करने वाली हरिणी है, तो दूसरे में वह अनेकता को जन्म देने वाली हरिणी है। इन दो हरिणियों की तुलना स्रुवा से की गई है। उन्हीं को दोनों जबड़े (शिप्रे) भी कहा
---------------------------------
1 यजुरित्येष हीदं सर्वं युनक्ति । (माश. 10 5.2.20)
2 तद् (ब्रह्म) यजुरित्युपासीत, सर्वाणि हास्मै भूतानि श्रेष्ठ्याय युज्यन्ते । (शां. आ. 4.6; कौ. 3.2.6)
3 एष (वायुः) हि यन्नेवेदं सर्वं जनयत्येतं यन्तमिदमनु प्रजायते तस्माद् वायुरेव
यजुः (माश. 10.3.5.1-2)
4 फतहसिंह : वैदिक दर्शन, पृ. 119 (भारती भण्डार, इलाहाबाद)
91
गया है और वे ही इंद्र के दो हरी भी हैं--
स्रुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दविध्वतः ।।
प्र यत्कृते चमसे मर्मृजद् हरी पीत्वा मदस्य हर्यतस्य अंधसः ।। ऋ. 10.96.9
इन दोनों हरिणियों का अद्वैत हरिणी रूप हिरण्ययकोश में प्राप्त होता है। अतः शौनकीय अथर्ववेद 10.2 हिरण्यय कोशस्य आत्मन्वत् ब्रह्मरूपी यक्ष की चर्चा1 करते हुए एक ऐसी जाज्वल्यमाना हरिणी का उल्लेख करता है जो यशोमण्डिता हिरण्ययी अपराजिता पुरी भी है –
प्रभ्राजमानां हरिणीं यशसा संवरीवृताम् ।
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ।। शौ. 10.2.33
अतः एकीभूत हरिणी अथवा हरि स्वयं इंद्र हरि है। हरि नामक योनि अथवा 'दिव्यं सदः वह है जिसे मनुष्य-व्यक्तित्व की नाम-रूपात्मक चेतनाएँ रूपी गायें अनेक हरितों द्वारा पूरित करती हैं और जिसे अन्यत्र चारों ओर प्रेरित करने वाले अनेक ‘हरयः' यहाँ केवल दो हरियों के रूप में परिणत होकर अंततः एक ‘हरि योनि' अथवा दिव्य सदस् बन जाते हैं। इस अद्वैत स्थिति को अरं नामक वह चरमावस्था कहा जाता है जिसे मनुष्य-व्यक्तित्व के अनेक चेतनाओं रूपी ‘हरयः' ध्रुव काम के लिए (कामाय स्थिराय) हरिद्वय होकर धारण2 करते हैं । यह काम वही है जिसे अथर्ववेद में ‘मनसः रेत:' तथा भगवद्गीता में धर्माविरुद्ध काम कहा गया है । यह अतीन्द्रिय काम है जो धारणा, ध्यान, समाधि द्वारा ब्रह्मानन्द की कामना के रूप में रहता है । यह वस्तुतः निष्काम अथवा अचाह की अवस्था है जो इंद्रियविषयों से सर्वथा पराङ्मुख होने पर ही उद्भूत होता है । यह अवस्था सभी कल्मषों, विषयवासनाओं को हरण करने वाली अद्वैत ‘हरिणी' कही जा सकती है। यही वह एक हरि है जो इंद्र के उन हरिद्वय की अद्वैत अवस्था है जिन्हें निघण्टु के ‘आदिष्टोपयोजनानि में इंद्र के हरिद्वय बताया गया है और जो स्वयं इंद्र से अभिन्न है ।
पुराणों का उच्चैःश्रवा और वैदिक हय :
पुराणों में यही वह उच्चैःश्रवा है जिस पर इंद्र आरूढ़ रहता है । इसका जन्म जिस समुद्र-मंथन से हुआ कहा जाता है वह वस्तुतः डॉ. फतह
---------------------------------
तस्मिन् हिरण्ये कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते ।
तस्मिन् यद् यक्षमात्मवत् तद् वै ब्रह्मविदो विदुः ।। शौ. 10.2.32
2 ऋ. 10.96.2
3 अरं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन् हरयो हरी तुरा।।
अर्वद्भिर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे ।। ऋ. 10.96.7
92
सिंह के अनुसार मनुष्य-व्यक्तित्व का चेतना-सिन्धु है। इससे निकलने वाले 14 रत्नों में से विष सबसे निकृष्ट है और अमृत सर्वोत्कृष्ट । अन्य 12 रत्न इन्हीं दो छोरों के बीच आते हैं। जैन-दर्शन के अनुसार, मनुष्यव्यक्तित्व के विकास के 14 विकासस्तर हैं जिन्हें गुणस्थान कहा जाता है । निकृष्टतम गुणस्थान मिथ्यात्व का है और सर्वोत्कृष्ट गुणस्थान ‘जिन अथवा तीर्थङ्कर का है। इन गुणस्थानों की तुलना डॉ. फतहसिंह ने अपने भारतीय समाजशास्त्र में 14 मन्वन्तरों से भी की है और उन्हें मनुष्यव्यक्तित्व के 14 विकासस्तर माना है । उच्चैःश्रवा का सर्वोच्च स्तर से सम्बन्ध प्रतीत होता है ।
वैदिक साहित्य में जब समुद्र को अश्व का बन्धु तथा योनि कहा जाता1 है, तो उसके उच्चैःश्रवा रूप से ही तात्पर्य हो सकता है। उसकी दो महिमाएँ मानी गई हैं जो चारों ओर प्रकट होती हैं, तो वह हय रूप में देवों का, वाजी रूप में गन्धर्वो का, अर्वा रूप में असुरों का तथा अश्व रूप में मनुष्यों का वाहक बनता2 है। इस प्रकार हय, वाजी, अर्वा तथा अश्व को उच्चैःश्रवा के ही रूपान्तर माना जा सकता है ।
इसका अभिप्राय है कि उच्चैःश्रवा अपने अर्वा रूप में असुरों से भी सम्बन्धित हैं । भागवत3 पुराण के अनुसार जब समुद्र-मंथन से उच्चैःश्रवा पैदा हुआ, तो असुरराज बलि ने उसको लेने की इच्छा प्रकट की और भगवान् की शिक्षा पाकर इंद्र ने उसे नहीं चाहा । फिर भी वह अश्व बलि के पास नहीं रह सका और अन्ततोगत्वा इंद्र के पास ही गया । इंद्र मनुष्यव्यक्तित्व के उच्चतर पक्ष का राजा है; अतः उच्चैःश्रवा भी उसके पास जाकर ही अपने नाम को सार्थक कर सकता है; परन्तु असुरपक्ष (राजा बलि) द्वारा उसे चाहना सम्भवतः उच्चैःश्रवा के उस रूप की ओर संकेत करता है कि जिसे वेद में औच्चैःश्रवा कहा गया । ये दो रूप ही शतपथ ब्राह्मण में वणित उच्चैःश्रवा की पूर्वोक्त दो महिमाएँ हो सकती हैं जिनमें से प्रथम देवों के लिए हय तथा गन्धर्वो के लिए वाजी में परिणत होती हैं, जबकि द्वितीय से असुरों के लिए अर्वा तथा मनुष्यों के लिए अश्व आविर्भूत होता है।
देवी भागवत महापुराण के छठे स्कन्ध के 18वें अध्याय में उच्चैःश्रवा की एक अन्य कथा आती है। सूर्य-पुत्र रेवन्त उच्चैःश्रवा पर सवार होकर विष्णु के दर्शन को गया। लक्ष्मी व उच्चैःश्रवा दोनों समुद्रमन्थन से उत्पन्न हुए। अतः दोनों बहिन-भाई हुए । लक्ष्मी जी उच्चैःश्रवा को देखती ही रह गई। विष्णु ने इस प्रकार
---------------------------------
1 माशब्रा 10.6.4.1
2 माशब्रा 10.6.4. 1
3 भा. पु. 8.8.3
93
मुग्ध होने का कारण लक्ष्मी से पूछा तो वह भी उत्तर न दे सकीं । विष्णु ने उसे उत्तरकुरु में बड़वा होने का शाप दिया । उत्तरकुरु में जाकर लक्ष्मी ने कालिन्दी-तमसा संगम पर पति-प्राप्ति के लिए तप किया। विष्णु ने हय का रूप धारण करके बड़वा रूपिणी लक्ष्मी को पत्नी बनाया तो उससे हैह्य नामक पुत्र हुआ । विष्णु ने अपने एक पुत्रहीन भक्त को पालनपोषण के लिए वह पुत्र दे दिया। भक्त का नाम तुर्वशु अथवा हरिवर्मन बताया जाता है । तुर्वशु ने उस हैहय का नाम एकवीर रखा । एकवीर ने राजा रेभ्य की पुत्री एकावली का उद्धार कालकेतु नामक दैत्य को मार कर किया और फिर उससे विवाह किया। कालकेतु की नगरी का पता लगाने और उसके वधनिमित्त विद्याएँ सीखने में एकावली की सखी यशोवती ने एकवीर की बड़ी सहायता की थी।
इस कहानी में उच्चैःश्रवा पर सवारी करने वाला सूर्यपुत्र रेवन्त है, परन्तु गर्ग-संहिता के विश्वजित् खण्ड में उच्चैःश्रवा पर चढ़कर शकुनि नामक असुर कृष्ण से युद्ध करने आता है। कृष्ण ने उसे पहले अश्व से नीचे गिराया, फिर कृष्ण तथा उनके सहयोगी योद्धाओं ने शकुनि को बाण मारते हुए उत्तरोत्तर भूमि से ऊपर ही रखा क्योंकि उसे वरदान था कि वह भूमि का स्पर्श करते ही जीवित हो जाएगा। भूमि-स्पर्श से वंचित करके ही उसका वध कर सके। इस प्रकार, उच्चैःश्रवा का सम्बन्ध जहाँ प्रकाश-प्रतीक रेवन्त से है, वहाँ अन्धकार-प्रतीक शकुनि से भी है । अतः उच्चैःश्रवा के दोनों पक्षों की तुलना शतपथ में वर्णित उसकी पूर्वोक्त दो महिमाओं से की जा सकती है-पहली महिमा देवों को वहन करने वाले हय तथा गन्धर्व वाहक वाजी रूप में प्रकट होती है तो दूसरी असुरवाहक अर्वा एवं मनुष्य वाहक अश्व में ।
हय
इसका तात्पर्य है कि हय आदि चतुर्विध अश्व उच्चैःश्रवा के ही रूपान्तर हैं। इनमें से देव-वाहक अश्व का नाम हय, डॉ. फतहसिंह के अनुसार, उस ज्ञानशक्ति का प्रतीक है जिसकी द्योतक 'विद्' धातु है । इसीलिए ऋग्वेद1 में विद्वान् की तुलना हय से की गई है। यजुर्वेद2 में जब 'वेदेन देवोऽसि' कह कर इस ज्ञानशक्ति को देवत्व का आधार माना गया तो इस प्रकारान्तर ज्ञानशक्ति रूपी हय को ही देववाहक स्वीकार कर लिया गया। हन् धातु से निष्पन्न ‘ह' तथा 'या' से निष्पन्न ‘य' के योग से निमित ‘हय' शब्द जिस द्विविध गति का सूचक है वह अन्तर्मुखी
---------------------------------
1 2
ऋ. 5.46.1
2 मा. सं. 2.21
94
बहिर्मुखी अथवा पराक्-अर्वाक् गति है जिसे प्राणापानौ के साथ आदि में देखा जा सकता है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जिन अश्विनौ1 का समीकरण श्रोत्रयुगल, नासिकारन्ध्र, प्राणापानौ के साथ किया गया है उसके लिए हय शब्द का सजातीय ‘हयन्ता'2 विशेषण प्रयुक्त होता है और जहाँ वे एक ओर दिवोदास के लिए गतिशील होते हैं, वहीं दूसरी ओर भरद्वाज के लिए भी गतिशील होते हैं—
यद् अयातम् दिवोदासाय वर्तिर् भरद्वाजाय अश्विना हयन्ता ।
रेवद् उवाह सचनो रथो वाम् वृषभः च शिंशुमारश्च युक्ता ।।ऋ. 1.116.18) ।
यहाँ अश्विनौ के रथ से जुड़े हुए वृषभ तथा शिंशुमार (एक थलचर, दूसरा जलचर) की जोड़ी अश्विनौ की द्विविधता की ओर संकेत करती है।
यह द्विविधता वैदिक देवों में से अधिकतर की कल्पना में पाई जाती है । उसके लिए देवमिथुन शब्द प्रयुक्त होता है –
तौ एव एतौ स्तोमौ अभवताम् । पराङ च । पूर्वाङ् च । तौ प्राणापानौ, तौ अहोरात्रे, तौ पूर्वपक्षापरपक्षौ, तौ इमौ लोकौ (द्यावापृथिव्यौ), तौ इन्द्राग्नी, तौ मित्रावरुणौ, तौ अश्विनौ, तद् दैव्यं मिथुनं यदिदं कि च द्वंद्वं तद्भवताम् ।। (जैब्रा 1.109)
यही दैव्यं मिथुनं' की प्रतीकात्मक कल्पना शतपथ ब्राह्मण के अश्वमेधप्रकरण3 में राजा की चार पत्नियों, एक कुमारी तथा सौ अनुचरियों के प्रसंग में पाई जाती हैं और प्रत्येक मिथुन में जब ‘हये-हये' कह कर महिषी
आदि को सम्बोधित किया जाता है तो उसका आधार ‘हय' शब्द की पृष्ठभूमि में स्थित उक्त द्विविधता ही हो सकती है। इसी प्रकार ‘हये देवाः4 कहकर प्रार्थना की जाती है कि “तुम्हारा रथ ऋत में ‘मध्यवाट न हो' जिसका अर्थ है कि देव द्विविध गति करें। ‘हये' पूर्वक मरुतः के सन्दर्भ में जब ‘अमृताः ऋतज्ञाः' के साथ ‘सत्यश्रुतः कवयः' भी कहा जाता है तो फिर ऋतञ्च सत्यञ्च' की जोडी स्मृतिपथ पर आ5 जाती है। इसी तरह जिस उर्वशी को ‘हये जाये'6 कहकर पुरुरवा पुकारता है वह भी स्वर्ग तथा पृथिवी दोनों ओर गति करने वाली है और इन्द्रियाः हया:7 भी ‘मेधाम् अभि प्रयांसि च' कहकर द्विविध गति से युक्त बताए जाते हैं ।
---------------------------------
1 तैसं 1.7.11.1; काठ. 13.5; माश. 12.9.1.13
2 ऋ. 1.116.18
3 माश. 13.5.2.1-2
4 ऋ. 2.29.4
5 ऋ. 5.57.8; 58.8
6 वही, 10.95.1
7 वही, 9.107.25; कौब्रा 1.522; जेब्रा 1.53.10
(95
इसका अर्थ है कि 'हय' वह चेतना-प्रवाह है जो ज्ञानशक्तियों रूपी देवों को दोनों की ओर ले जाता है । हय के दो गन्तव्यों में से एक मनुष्यव्यक्तित्व का ‘पर' पक्ष है और दूसरा अपर । प्रथम को हय का शिर कहा जा सकता है तथा दूसरे को धड़ । हय का शिर मेधापरक(ऋ. 9.107,25) तथा धड़ अन्न (प्रयांसि) परक है। इसी हय के शिर द्वारा दधीचि ने अश्विनौ को वह विद्या बतला दी जिसे दधीचि को इन्द्र ने प्रदान करके कह दिया था कि यदि किसी अन्य को बताओगे तो तुम्हारा शिरच्छेद हो जाएगा।1 इस विद्या को खिलसूक्तों में सोमधान2 तथा उपनिषद् में मधुदिद्दा कहा गया है। सोम और मधु दोनों ही शब्द आनन्द-तत्त्व के वाचक है। इसलिए यह विद्या निःसन्देह उस ब्रह्मानन्द की प्राप्ति का मार्ग है जिसका अनुसरण ज्ञानी भगवद्भक्त करते हैं। अतः जिस हय-शिर से उसका उपदेश होता है उसे ज्ञानमूलक श्रद्धाशक्ति पर आश्रित समाधि का प्रतीक माना जा सकता है। इस शिर का उपयोग दधीचि ही नहीं करते, अपितु अश्विनौ से भी प्रार्थना की जाती है कि 'हे अश्विनौ ! जिसके द्वारा देवों ने पाप का नाश किया, जिसके द्वारा उन्होंने अदैवी (आसुरी) शत्रुओं का वध किया और जिसके द्वारा वे अमर हो गए वह सोमधान हमें हयशिर के द्वारा प्रदान करो।'
अतः हय को मनुष्यचेतना का विज्ञानमूलक भावपक्ष कह सकते हैं। इसका 'पर' पक्ष हयशिररूपी समाधि हैं जिसका मूल वह काम है जिसे वेद में मन का रेतस् कहा गया है और भगवद्गीता में ‘धर्माविरुद्ध' काम । इसका अपर पक्ष (जिसे हय का धड़ कहा गया) उसे भावपक्ष कह सकते हैं। जिसका आधार सेन्द्रिय मन:केन्द्रित काम है । दोनो स्तरों पर यह हयरूपी बिज्ञानचेतनापक्ष एक सद्यःस्फूर्ति और स्वत:स्फूर्ति वाला स्वभाव है। इसीलिए उससे तुलना ऐसे विद्वान् की, की गई है जो स्वयं ही उत्तरदायित्व से जुड़ जाता है, कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता5 । सेन्द्रियमन के स्तर पर तो उस हय पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन हो जाता है । इसीलिए उपनिषत् के एक रूपक में आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि, मन को लगाम, इंद्रियों को हय तथा विषयों को गोचर मानते हुए, आयुक्त मन वाले और विज्ञानरहित व्यक्ति के लिए इंद्रियों को वश में रखना वैसा ही कठिन माना है जिस प्रकार एक सारथि के लिए दुष्ट अश्वों पर नियंत्रण6
---------------------------------
1 खि. 1.113. 3
2 वही, 9.11.3; 11.9.4
3 बृउ 2.5.19; माशब्रा 4.1.5.18; 14.3.4.13
4 पादटिप्पणी 5
5 हयो न विद्वाँ अयुजि स्वयं धुरि । ऋ. 5.46.1.; शांब्रा 22.1
5 कठोपनिषद् 1.3.3-5
96
रखना । इसके विपरीत, जो व्यक्ति विज्ञानवान् तथा युक्त मन वाला होता है वह अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण रखता हुआ परमपद को प्राप्त करता है--
यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ।
तस्येन्द्रियाणि वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ।।
यस्तु विज्ञानवान् भवति समनस्क: सदा शुचिः ।
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद् भूयो न जायते ।। कठोपनिषद् 1.3.6; 8
विज्ञान जिसका सारथि है और मन रूपी लगाम पर जिसका नियंत्रण है, वही नर यात्रा पूरी करके विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है --
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः ।
सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ।। कठोप. 1.3.9
वाजी और गन्धर्व :
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य व्यक्तित्व के जिन दो पक्षों को क्रमशः उन्मनी और समनी शक्तियों से सम्बन्धित माना जा सकता है वे दोनों विज्ञानमयकोश के स्तर पर उच्चैःश्रवा के दो रूपान्तर कहे जा सकते हैं। इन दोनों में से पररूप को हय का शिर तथा अपर रूप को हय का धड़ कहा गया है; परन्तु यही सेन्द्रिय मन के स्तर पर उन शक्तियों को वहन करने वाला प्रतीत होता है जिन्हें वेद में गन्धर्वाप्सरसः नाम दिया गया है। अतः इस दृष्टि से उच्चैःश्रवा को उस वाजी में रूपान्तरित माना जा सकता है, जो गन्धर्वो का वाहक कहा गया है ।
इस प्रसंग में वाजी का विस्तृत विवेचन करने से पूर्व गन्धर्वाप्सरसः के स्वरूप को समझ लेना भी आवश्यक है । अतः यहाँ तैत्तिरीय आरण्यक से निम्नलिखित उद्धरण के साथ इस विषय का विवेचन प्रारम्भ किया जाता है ।
'अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः ।
देवी मेधा मनुष्यजा सा मा मेधा सुरभिर्जुषताम्।। तै.आ.10-41
इससे स्पष्ट है कि दैवी (ब्राह्मी) मेधा ही अप्सराओं की मेधा तथा गन्धर्वो के मन रूप में मनुष्यजा तथा सौरभमयी होती है। मेधा की यह गन्ध ही गंधर्वाप्सरसः की वह प्रिय गंध है जो सूर्या-विवाह के रूप में कल्पित एक आध्यात्मिक घटना से जुड़ी हुई है—
यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मा सुरभिं कृणु । मा नो द्विक्षत कश्चन । यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजभ्रु सूर्याया विवाहे ।
97
अमर्त्याः पृथिवि गन्धमग्रे तेन सुरभिं कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन । ।
शौ 12.1.23-24
यह गन्ध जिस पृथिवी से मिलती है वह वस्तुत: वही विराज गो है जिसे गन्धर्वाप्सरस पुण्यगंध कह कर बुलाते हैं, क्योंकि वे उसी से प्राप्त पुण्यगन्ध पर आश्रित1 हैं। इस पुण्यगंध को देने वाली पृथिवी अथवा विराज गौ को पृथिवी नामक ग्रह समझना भूल होगी। यह भूमि अथवा पृथिवी हमारे भीतर स्थित वह शक्ति है जिसका अमृत हृदय परम व्योम2 नामक अन्तश्चेतना स्तर पर सत्य से आवृत3 है। यह हमारी वाक् नामक आध्यात्मिक शक्ति है । ‘वाग्वै विराज्' (मै. सं. 3.2.10, जै.ब्रा. 3.67, मा.श. 3.5.1.14) कह कर उसी के पुण्यगंधवती विराज होने की पुष्टि की गई है और इसी मत को कपिष्ठलकठ में (4/2) पृथिवी-विराज के तादात्म्य द्वारा समर्थन दिया गया है ।
अतः गंधर्वाप्सरस का उपजीव्य गंध एक अध्यात्मिक निधि है । वह न केवल नर-नारियों में भग नामक ज्योति के रूप में, अपितु अश्वों, वीरों, मृगों, हस्तियों एवं कन्याओं के वर्चस् के रूप में व्याप्त होती है, वह जिसमें होती है उससे कोई द्वेष नहीं करता4। इसका तात्पर्य है कि वह गंध प्रेम का आधार बनती है । आधुनिक कामशास्त्रियों की मान्यता है कि कामभावना से ओत प्रोत प्राणी में एक प्रकार की गंध निकलने लगती है; परन्तु यह अनुभवसिद्ध बात है कि कुछ योगियों के आस-पास भी एक नैसर्गिक गंध रहती है जिसकी पूर्ण अभिव्यक्ति तभी होती है जब व्यक्ति में उस वासनारहित काम का विकास होता है जिसे मनसः रेत:' (शौ. 19, 52.1) कहा जाता है। पूर्वोक्त विराज् को उसी काम की दुहिता कह कर धेनु रूप में (शौ. 9.2.5) कल्पित किया जाता है। व्यक्ति में जब यह उग्र काम अध्यक्ष बनता है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक शत्रुओं से रहित होकर
---------------------------------
1 सोदक्रामत् सा गन्धर्वाप्सरस अगच्छत तां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वन्त पुण्यगन्ध एहीति । तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत् पुष्करपर्णं पात्रं । ता वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक् । तां पुण्यमेव गन्धमधोक् । तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति । शौ 8.10(5).4-8
2 देखिए आगे 'व्योम'
3 यस्या हृदयं परमे व्योमन् सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः ।
सा नो भूमिस्त्विषिं बलं राष्ट्रे दधातूत्तमे । शौ 12.1.8
4 यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः ।
यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषूत हस्तिषु ।
कन्यायां वर्चो यद् भूमे तेनास्मान् अपि संसृज मानो द्विक्षत कश्चन ।।। शौ 12.1.251
98
विश्वे देवाः और सर्वे देवाः नामक प्राणों द्वारा समान रूप से लाभान्वित होने लगता1 है। इसी का 'त्रिवरुथ शर्म' ब्रह्म वर्म होकर व्यक्ति में प्रसार पाता है, तो उसके शत्रुओं का विनाश तथा जीवन की रक्षा2 होती है ।
ऊर्ध्व-गन्धर्व :
इसी काम को कान्त्यर्थक वेन धातु से निष्पन्न वेन नाम भी दिया गया है । वेन (काम) ही ऊर्ध्व गन्धर्व (ऋ. 10.123.7) है जो ‘सुरभि (गंध) को धारण करके ‘प्रियाणि' को उत्पन्न कर सकता है । गन्धर्व की इन प्रिय उपजों अथवा अभिव्यक्तियों की मूल सत्ता को ही वह एक ‘अप्सरा' कहा जाता है जो अपने ‘जार' (गन्धर्व) को परम-व्योम में धारण करती3 है । अत: गन्धर्व को यदि मूल कामानुभूति कहें, तो अप्सरा मूल कामाभिव्यक्ति होगी। मूल गन्धर्व एवं अप्सरा के विभिन्न रूपान्तरों को ही गन्धर्वाप्सरसः के नाम से जाना जाता है। मूल गन्धर्व और अप्सरा का अव्याकृत रूप द्रप्स (द्र+प्स) अर्थात द्रवणशील रूप है जो मन रूपी समुद्र को प्राप्त होकर गृध्र-दृष्टि (वासना दृष्टि) द्वारा देखता हुआ पूर्वोक्त ‘प्रियाणि' अप्सराओं को प्रकाशित करता है—
द्रप्स: समुद्रमभि यज्जिगाति पश्यन्गृध्रस्य चक्षसा विधर्मन् ।
भानुः शुक्रेण शोचिषा चकनस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाणि ।। ऋ. 10.123.8
मन रूपी समुद्र और उसकी तरंगों (आपः) के सन्दर्भ से ही अप्सराओं से सम्बद्ध गंधर्वो को प्रायः समुद्रेष्ठाः अथवा अप्सुस्थिताः (शौ. 2.2.3; 4.37.12) कहा जाता है और अप्सराओं (तरंगों) को समुद्र से आने-जाने वाला बताया जाता है। दूसरे शब्दों में, कामानुभूतियों (गंधर्व) और कामाभिव्यक्तियों (अप्सराएँ) का उद्गम और अवसान मनस्समुद्र में ही है। इसीलिए मनो गन्धर्वः (माश. 9.4.1.12) अथवा प्राणो वै गन्धर्वः (जैमिनीय उपनिषद् 3.6.8.3) जैसी उक्तियाँ वैदिक साहित्य में मिलती हैं। काम समुद्र के समान अपरिमित4 है, अतः कामानुभूति को समुद्र रूप में कल्पित करके कामाभिव्यक्तियों रूपी अप्सराओं को
---------------------------------
1 अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।
विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा हवमायन्तु म इमम् । शौ 9.2.7
2 यत् ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्भु ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यं कृतम् ।
तेन सपत्नान् परि वृङ्ग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ।। शौ 9.2.16
3 अप्सरा जारमुपसिष्मियाणा योषा बिभर्ति परमे व्योमन् । ऋ. 10,123.51
4 समुद्र इव हि कामोऽपरिमितः । काठ. 9.12
99
आपः1 कहा जाता है ।
साधु और असाधु गन्धर्वाप्सरसः
गन्धर्व और अप्सरस अच्छे-बुरे दोनों प्रकार के होते हैं । विभिन्न संहिताओं और वैदिक ग्रन्थों में गन्धर्व और अप्सरसः साधु-असाधु दो प्रकार के प्राप्त होते हैं। गन्धर्वो के लिए दिव्य, ऊर्ध्व, वायुकेश, भद्र, सोमरक्षक आदि अनेक विशेषण आते हैं। इन विशेषणों में दिव्य विशेषण का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए जैमिनीय उपनिषद् ब्राह्मण (3.5.6, 1, 2, 4) में गन्धर्वों को दिव्य कहा गया है तथा ऋग्वेद (10.139.5) में विश्वावसु को (मै. सं. 4.9, 1) तथा तै.आ (5.9.22) में किसी रति नामक दिव्य गन्धर्व का कथन हुआ है। अन्यत्र विभिन्न देवताओं के लिए दिव्य गन्धर्व पद अनेकशः आया है। ऋ. 5.86.36 में सोम को और मा. सं. 9.1, 11.7, 30.1, का. 10.1.1, 12.1.7, 34.1.1. तै. 1.7.7.1, 4.1.1.6, मै. 1.11.1, काठ. 13.14, 15.11 और माश. 5.1.1.16 में सविता-देव को दिव्य गन्धर्व कहा गया है ।
अप्सराओं को द्विविध साधुता :
अथर्ववेद के एक सूक्त (शौ. 4.38) में जिन द्विविध साधु अप्सराओं का वर्णन है उससे यही संकेत मिलता है कि वे कोई हाड़-मांस की स्त्रियां नहीं, अपितु मनोवैज्ञानिक सत्ताएँ हैं। इनमें से एक (वही, 1) प्रकार की अप्सराओं की साधु-देविनी (अच्छा जुझा खिलाने वाली) संज्ञा दी गई है और दूसरी को सूर्यरश्मियाँ अथवा मरीचियाँ (वही, 5) कहा गया है। जुए में कुल पाँच अक्ष (पाँसे) होते थे जिनको ‘अयाः' कहा जाता था। उनमें से प्रथम चार की ‘कृतम्' संज्ञा होती थी और पञ्चम को ‘कलि कहा जाता था। ये अक्ष वेद में ज्ञानेन्द्रियों के प्रतीक प्रतीत होते हैं। इन्द्रिय-विषयों में आसक्त पञ्च-कर्मेन्द्रियों की समष्टि, एक स्पर्श नामक ज्ञानेन्द्रिय के ही पंच भेद होने से ‘कलि' संज्ञा ग्रहण करती है । इसे छोड़कर ‘कृतम्' नामक अन्य चार की समष्टि को प्राप्त करना ही विजय का सूचक समझा जाता था। इन्द्रिय रूपी अक्षों के व्यापार में ‘कृतम् द्वारा विजय दिलाने का जुआ जिस वासना की अभिव्यक्ति प्रदान करता है वह ‘साधुदेविनी’ अप्सरा कही गई है, क्योंकि शोक एवं क्रोध को धारण
---------------------------------
1 तु. आपो वे सर्वे कामाः । माश. 10.5.4.15
अपोऽप्सरसः । माश. 9.4.1.10
2 एकादय: पंचसंख्यान्ता अक्षविशेषाः अपाः। तत्र चतुर्णां कृतम् इति संज्ञा
(सा. भा. शौ. 4.38.3) अथ ये पंच लिः सः (तै ब्रा 1.5.11.11)
100
करती हुई वह ‘आनन्दिनी प्रमोदिनी अप्सरा' है --
या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिभ्रती ।। आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ।। (शौ. 4.38.4)
इस साधुदेविनी अप्सरा से भी श्रेष्ठ वे मरीचि नामक अप्सराएँ हैं। जो परब्रह्म परमात्मा रूपी सूर्य की रश्मियों का अनुसरण करती हैं। उनका नियामक ब्रह्मज्ञान की वाजिनी उषा से युक्त जीवात्मा है । उसकी कल्पना वृषभ रूप में की है --
सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति ।
यासामृषभो दूरतो वाजिनीवान्सद्यः सर्वान् लोकान् पर्येति रक्षन् ।। (शौ. 4.38.5) इन्हीं मरीचियों से सम्भवतः वह उषा बनती है जिसे वाजिनी कहते हैं । वाजिनी उषा से युक्त होने के कारण जीवात्मा को वाजिनीवान् कहा जाता है। वह अपने सम्पूर्ण अंतरंग लोक (अन्तरिक्ष) के साथ आकर मनुष्य की शुभ्रवाक् का रक्षक बनता है। वास्तव में यह वाक् उसी की बछिया (वत्सा) है। उसकी रक्षा जब उक्त आत्मा करने लगता है, तो मानसिक चेतना की अनेक धाराएँ एकीभूत हो जाती हैं जिससे मनुष्य का मन भी आत्मलीन हो जाता है अर्थात् उसकी अनेकोन्मुखी चञ्चलता एकाग्रता में बदल जाती है --
अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन् कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।
इमे ते स्तोका बहुला एहि अर्वाङियं ते कर्कीह ते मनोऽस्तु ।। (शौ. 4.38.6)
इसका यह अभिप्राय नहीं कि उक्त मरीचि नामक अप्सराओं अथवा वाजिनी उषा से युक्त होकर जीवात्मा भोग अथवा कर्मों को सर्वथा त्याग देता है । अगले मन्त्र में भोग को घास के रूप में और कर्मक्षेत्र को वज्र के रूप में कल्पित करते हुए कहा गया है कि उक्त उषा से युक्त जीवात्मा जब अपने समस्त अंतरंग लोक द्वारा वाक् रूपी बछिया की रक्षा करने लगता है तो उस पर इतना नियन्त्रण हो जाता है कि उसके कुपथ पर जाने की सम्भावना ही नहीं रहती--
अयं घासो अयं वज्र इह वत्सां नि बध्नीमः ।।
यथानाम व ईश्महे स्वाहा ।। (शौ. 4 38.7)
गन्धर्वाप्सरसः के भेद
इस प्रकार अप्सराओं को तीन श्रेणियों में रखा हुआ माना जा सकता है। इनमें से एक तो उपद्रव कारी असाधु अप्सराएँ हैं। दूसरी
101
साधुदेविनी अप्सराएँ हैं जो साधु होती हुई भी क्रोध और भय को उत्पन्न करने वाली कही गई हैं। तीसरे प्रकार की अप्सराएँ दिव्य अप्सराएँ कही
जा सकती हैं। इन्हीं को ऊपर ‘मरीचयः' कहा गया है।
अप्सराओं की त्रिविधता के समान ही अच्छे बुरे गन्धर्वो की त्रिविधता भी प्रसिद्ध है । इस प्रसंग में अथर्ववेद का निम्नलिखित मन्त्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है --
श्वेवैक: कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः ।
प्रियोदृशइव भूत्वा गन्धर्वः सचते स्त्रियस्तिमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता ।। (शौ. 4.37.11)
यहां गन्धर्व के जो ये तीन रूप हैं, वे सभी उपद्रवकारी हैं, क्योंकि इनको अवांछनीय समझा गया है। कुत्ता, कपि और सर्नकेशक कुमार कहे जाने वाले इस त्रिविध गन्धर्व से क्रमश पेट, हृदय तथा मस्तिष्क से सम्बन्धित वासना का ग्रहण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अग्नि, वायु और आनन्द से भी तीन गंधर्व माने गए हैं। इनका सम्बन्ध क्रमशः पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यौ से माना (जै ब्रा. 2.241) गया है। व्यक्ति में अन्नमय, प्राणमय को पृथिवी, मनोमय को वायु एवं विज्ञानमय को द्यौ कह सकते हैं।
अन्य कई दृष्टियों से गन्धर्वो के 11 गण हैं जिनके नाम तैत्तिरीय आरण्यक में स्वान, भ्राट्, अंगारि, बम्भारि, हस्त, सुहस्त, कृशानु, विश्वावसु, मूर्धन्वान्, सूर्यवर्चा तथा कृति (तै. आ. 1.9 3) बताया जाता है। यजुर्वेदीय परम्परा में गंधर्वों की संख्या 27 बताई गई है। (तैसं 1.7.77.2, मै.सं. 1.11.1, माश. 5.1.4.8)।
गन्धर्वाप्सरसः राष्ट्रभृतः
यद्यपि गंधर्वो के उक्त वर्गीकरण की समुचित व्याख्या का कोई सूत्र नहीं दिखाई पड़ता; परन्तु ये सभी साधु अथवा भद्र गंधर्व प्रतीत होते हैं। इन्हीं की गणना ‘राष्ट्रभृतः गंधर्वाप्सरस:' (तैसं. 3.4.8.4) में मानी जा सकती है क्योंकि राष्ट्र का भरण-पोषण करने वाले गंधर्वाप्सरसः निःसन्देह भद्र होंगे। गंधर्वाप्सरसः जिस लोक की रक्षा करने वाले हैं उसको ऋतधाम (जैब्रा. 3.348) कहा जाता है । ऋत वेद में नैतिक व्यवस्था का आधारभूत तत्त्व है । अत: जो गंधर्वाप्सरस: राष्ट्रभृत् और ऋतधाम के रक्षक कहे जाते हैं वे कामानुभूति तथा कामाभिव्यक्ति की वे ही प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं जो ऋत के अनुकूल हों। ‘मातृवत्परदारेषु' जैसी उक्तियों का आधार कामानुभूति एवं कामाभिव्यक्ति की यह ऋत
102
नामक नैतिक व्यवस्था ही रही होगी। विवाह, एकपत्नीव्रत, पतिव्रत आदि कामवासना को नियन्त्रित करने वाले आदर्श गन्धर्वाप्सरसः के इसी राष्ट्रभृत् रूप की ओर संकेत करते हैं ।
अश्वमेध के अश्व से सम्बन्धित गन्धर्व भी उनके राष्ट्रभृत् रूप की ओर इंगित करते हैं क्योंकि राष्ट्रं वै अश्वमेधः' (माश. 13.2.2.16) के अनुसार अश्वमेध राष्ट्र का प्रतीक है। तैत्तिरीय संहिता में अश्व से युक्त होने वाले 27 गन्धर्व हैं जो उसे गति (जव) प्रदान (तैसं. 1,7,7,2) करते हैं। यही बात मैत्रायणी संहिता (1,11,1) में भी कही गई है। इन 27 गन्धर्वो का सम्बन्ध वहाँ वायु अथवा मनु से भी बताया (तै. सं. वही) गया है। अतः इन गन्धर्वो के स्वरूप का निर्धारण मनु और वायु के सन्दर्भ में जान लेना आवश्यक है।
मनु, वायु और गन्धर्व :
मनु के साथ समीकृत होने से 27 गन्धर्व निस्सन्देह व्यष्टिगत कामानुभूति के 27 प्रकार सिद्ध होते हैं। मनु जीव का वह रूप है जो ऊर्ध्वमना होकर मनन करता है। इसका अर्थ है कि मन का सम्पर्क केवल अहंबुद्धि से ही नहीं, अपितु महत् बुद्धि और प्रधान (मूल प्रकृति) से भी हो जाता है। इस प्रकार निम्नलिखित रूप में मनुष्य की चेतना में तीन स्तरों पर प्राणों का नवीकरण हो जाता है—
1 प्रधान, महत् बुद्धि, अहंबुद्धि, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ।
2 प्रधान, महत बुद्धि, अहंबुद्धि, मन और पाँच स्थूल प्राण ।
3 प्रधान, महत् बुद्धि, अहंबुद्धि, मन और पाँच कर्मेन्द्रियाँ ।
इन्हीं 27 रूपों के संदर्भ में मूल काम भी 27 गन्धर्वो के रूप में कल्पित किया जाता है। कभी-कभी इन्हीं को वैदिक मनोविज्ञान में 27 नक्षत्र कहा जाता है और इन्हीं के प्रतीकस्वरूप आकाशीय नक्षत्रों की कल्पना की जाती है ।
मननशील जीव रूपी मनु इन 27 गन्धर्वो की सृष्टि तभी कर सकता है जब ऊर्ध्वमना होकर अर्जित की हुई शक्ति को वह व्युत्थान की अवस्था में मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमय स्तरों पर पहुंचता है। अतः इस रूप में, वह मनुष्य की समस्त पंचकोशीय विभूतियों को एकजुट कर लेने से वायु कहलाता है- यदिदं सर्वं युते तस्माद् वायुः' (जै. 2.26.) । दूसरे शब्दों में आनन्दमयादि कोशों के क्रमशः विद्युत्, वृष्टि, चन्द्रमा एवं अग्नि कहलाने वाली देवताएँ (देवशक्तियाँ) इस वायु को सर्वथा भरपूर (ऐ. ब्रा. 8 24) करती हैं। अतः इस रूप में मननशील जीव (मनु) एक ओर तो 'वायुः
103
मध्यमा विश्वज्योतिः' (माश 8.3.2.1) बनता है, तो केवल आनन्दमय कोश के सन्दर्भ से मूल प्रेरक एवं स्रोत होने से सविता (गो. 1.1.33; जै. उ. 8.12.15) कहलाता है और इसी रूप में ‘वायुर्वै शान्तिः ' (जै 2. 138; 3.66) की उक्ति भी चरितार्थ करता है ।
अश्व और गन्धर्व :
अतः मनु अथवा वायु से समीकृत उक्त 27 गन्धर्वो को अश्व के लिए वेग प्रदान करने वाला कहा जाता है, तो अवश्य ही यह अश्व किसी आध्यात्मिक तत्व का प्रतीक माना जाएगा। बृहदारण्यक उपनिषद् एक ‘मेध्य अश्व' के उल्लेख से प्रारम्भ होती है, तो उषा को उसका सिर कहा है। इसने हय होकर देवों को, वाजी होकर गन्धर्वों को, अर्वा होकर असुरों को और अश्व होकर मनुष्यों को वहन किया (बृ. उ. 1.1.2)। ये देव, गन्धर्व, असुर एवं मनुष्य सम्भवतः चतुर्विध प्राण हैं जिनकी अनेकता का जन्म क्रमशः विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमयकोश में माना जा सकता है । मनुष्य बहिः प्राण (तै. सं. 6.1.1.4) कहा जाता है, क्योंकि अपने अन्नमयकोश के माध्यम से ही उसकी चेतना सामाजिक व्यवहार द्वारा बहिर्मुखी अश्वत्व (व्यापकत्व) प्राप्त करती है । इसीलिए बहिमुखी व्यक्तित्व ही वह अश्व है जो मनुष्य को वहन करने वाला कहा गया।
इस प्रसंग में, स्मरणीय है कि यह बात 'मेध्य अश्व' के विषय में कही गई है । जो मेध्य अर्थात् मेधापूत है। वह उस मेधा से सम्बन्धित है जिसकी उपासना देव, पितर आदि करते हैं (मा. 32.14)। इस मेधा के बिना तो मनुष्य-व्यक्तित्व मेध्य अश्व के स्थान पर अनृतसंहिता (ऐ. ब्रा. 1.6) का रूप ले लेता है । सायण के अनुसार आत्मा और ब्रह्म का अभेद ज्ञान सुलभ कराने वाली बुद्धि का नाम मेधा है (तै आ. 10 .39) ।। अतएव यह ज्ञानज्योतिर्मयी मेधा ही वह उषा हो सकती है जो मेध्य अश्व का पूर्वोक्त शिर मानी गई है। इस मेधा का मूलस्थान हिरण्ययकोश है, क्योंकि वहीं पर ब्रह्मात्मसायुज्य (अ. वे. 10.2.32) की स्थिति मानी गई है । यही मेधा अथवा मेधात्मक मन अप्सराओं और गन्धर्वो में पाई जाने वाली दैवी मेधा कही गई है जो निस्सन्देह ‘मनुष्यजा' अर्थात् मनुष्य के भीतर ही साधना द्वारा उत्पादनीय है -
अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः ।
दैवी मेधा मनुष्यजा सा मां मेधा सुरभिर्जुषताम् ।। तै.आ. 10.41
यही मनुष्यजा मेधा मनुष्य को यशसुरभि प्रदान करती है, क्योंकि इसके कारण उसका सामाजिक व्यवहार दिव्य बन जाता है। दूसरे शब्दों
104
में यह मेध्य अश्व सामाजिक दृष्टि से अपराजेय होकर ऐसे अश्वमेध राष्ट्र का निर्माण करता है, जहाँ अमेध्य, अभद्र और अदेवत्व का नाम नहीं रहता । उक्त मनुष्यजा मेधा पर आश्रित यह मेध्य अश्व वस्तुतः ‘देवयान है जिसके चतुर्दिक् ले जाने वाले मनोमय, प्राणमय एवं अन्नमय नामक तीन मानुष स्तर हैं (ऋ.1.162.4) अतः इस अश्व नामक मनुष्य-व्यक्तित्व को व्यापकत्व (अश्वत्व) देने वाले मानुष व्यक्तित्व के ये तीन स्तर ही हैं।
इस मेध्य अश्व का सर्वोच्च जन्मस्थान (परमं जनित्रं ऋ. 1.163.4) वही ब्रह्मात्मसायुज्य वाला हिरण्ययकोश है जहाँ पूर्वोक्त मेधा मूलतः उपजती है । इस कोश में स्थित चेतन-तत्त्व ही वह ‘सूर' है जिससे इस अश्व का तक्षण (ऋ. 1.163.2) किया जाता है। सूर से अश्व को प्राप्त करना कोई सरल काम नहीं । बार-बार मनुष्य उसके लिए वासना करता है, अश्व को चाहने वाली यह वासना प्रतिबार एक उत्कृष्ट रूप धारण करके ‘सूर' के पास जाती है । वासना के इन अनेक रूपों को ही ‘वसव' (ऋग्वेद,वही) कहा गया है जो अश्व को 'सूर' से तक्षण करके निकलते हैं।
अश्व की जायमान अवस्था का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि वह हिरण्ययकोश रूपी समुद्र और विज्ञानमयकोश रूपी 'पुरीष' से ऊपर उठता है (ऋ. 1.163 11) । वेग के कारण उस समय उसे श्येन के समान दो पङ्खों से उड़ता हुआ अथवा हरिण के समान अपनी बाहुओं से छलांगता हुआ (वही) कह सकते हैं। इस प्रसंग में जिस अश्व के दो पङ्ख और दो बाहुएँ कही गई हैं वह पूर्वोक्त उच्चैःश्रवा अश्व ही है जिसकी चार महिमाओं का उल्लेख किया गया है। इन चार में से दो महिमाओं को अश्व के पङ्ख के रूप में तथा शेष दो को बाहुद्वय के रूप में कल्पित किया गया प्रतीत होता है। प्रथम दो महिमाएँ, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, क्रमशः देवों और गन्धर्वो की वाहन मानी गई हैं। गन्धर्व अपने साधुरूप में देवकोटि में ही परिगणित होते हैं और असाधू रूप में असुरत्व के निकट पहुंच जाते हैं । गन्धर्वों को वहन करने वाले उच्चैःश्रवा का जो रूप है, उसको वाजी कहा गया है । अतः वाजी साधु गन्धर्वों के प्रसंग में देववाहक कहा जाएगा । वाजी के इस दिव्य रूप का वर्णन अगले अध्याय में किंचित् विस्तार के साथ किया जा रहा है।
---------